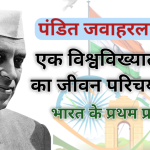नेताजी सुभाष चंद्र बोस: अदम्य देशभक्त और भारत की स्वतंत्रता की उनकी ललक
सुभाष चंद्र बोस जिन्हें प्यार से नेताजी’ कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सबसे प्रबल, करिश्माई और विवादास्पद व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनका जीवन अटल संकल्प, क्रांतिकारी कार्रवाई और इस दृढ़ विश्वास का प्रमाण था कि आज़ादी भीख में नहीं, बल्कि बलपूर्वक ली जानी चाहिए।
महात्मा गांधी के अहिंसक सत्याग्रह से चिह्नित आंदोलन में, बोस एक सैन्यवादी दृष्टिकोण के शक्तिशाली पैरोकार बने जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा रहस्य में डूबी उनकी असामयिक मृत्यु ने उनकी गाथा को और बढ़ा दिया, जिससे वे राष्ट्रवादी जोश और बलिदान का एक स्थायी प्रतीक बन गए।
प्रारंभिक जीवन
सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को कटक, ओडिशा में जानकीनाथ बोस, एक धनी और प्रमुख वकील, और प्रभावती देवी के घर हुआ था। वे एक बड़े, संपन्न बंगाली परिवार में चौदह बच्चों में नौवें थे। उनके पिता उच्च कद के व्यक्ति थे, जिन्हें “राय बहादुर” की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और उनकी माँ गहरी धार्मिकता और मजबूत चरित्र वाली महिला थीं, जिनके मूल्यों ने युवा सुभाष को गहराई से प्रभावित किया।

छोटी उम्र से ही, बोस ने स्वतंत्रता की एक प्रबल भावना और गहन देशभक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में शुरू हुई, और उसके बाद रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में। इसी दौरान राष्ट्रवाद के बीज बोए गए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत प्रचलित नस्लीय भेदभाव को देखा, जिसने उनकी चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी।
1913 में, वह कलकत्ता (अब कोलकाता) चले गए और प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी कॉलेज में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। हालाँकि, उनकी शैक्षणिक यात्रा जल्द ही एक निर्णायक घटना से बाधित हो गई। 1916 में, उन्हें एक ब्रिटिश प्रोफेसर, ई.एफ. ओटेन पर हमला करने के लिए निष्कासित कर दिया गया, जिसने भारतीय छात्रों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियाँ की थीं। यह घटना अन्याय को सहन करने से इनकार करने और सीधे अधिकार का सामना करने की उनकी इच्छा का एक स्पष्ट प्रारंभिक संकेत था।
बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री पूरी की, और फिर, अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए, 1919 में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, चौथा सर्वोच्च अंक हासिल किया और एक पद सुरक्षित किया
। हालाँकि, अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसमें सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों ने गोली मार दी थी, का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन के लिए विशेषाधिकार और सेवा का जीवन और अपने राष्ट्र की पुकार के बीच फटे, उन्होंने एक निर्णायक विकल्प बनाया। अप्रैल 1921 में, उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया, अपने भाई को लिखा, “अन्याय की सरकार को समाप्त करने का एकमात्र तरीका सरकार को ही समाप्त करना है।”
राजनीति में प्रवेश और कांग्रेस में उदय
भारत लौटने पर, बोस तुरंत राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। वे चित्तरंजन दास के गतिशील नेतृत्व की ओर आकर्षित हुए, जो एक उत्साही राष्ट्रवादी थे और उनके राजनीतिक गुरु बने। स्वराज पार्टी में दास के मार्गदर्शन में, बोस ने राजनीतिक संगठन की जटिलताओं और हिंदू-मुस्लिम एकता के महत्व को सीखा। वह दास के मेयर के रूप में कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने, जिससे उन्हें मूल्यवान प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ।
इस कारण के प्रति उनके समर्पण ने जल्द ही उन्हें एक प्रमुख युवा नेता बना दिया, लेकिन इसने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के साथ लगातार टकराव भी पैदा कर दिया। 1921 और 1941 के बीच, उन्हें ग्यारह बार जेल में डाला गया, जिसमें उन्होंने भारत और मांडले, बर्मा (म्यांमार) में विभिन्न जेलों में कुल सात साल से अधिक समय बिताया। इन कैद के दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया।
1920 और 1930 के दशक के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर बोस का कद लगातार बढ़ता गया। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने, जहाँ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया। हालाँकि, बोस और कांग्रेस के प्रमुख गांधीवादी धड़े के बीच एक मौलिक विचारधारात्मक दरार विकसित हो रही थी।
बोस का मानना था कि गांधी की अहिंसा और एक समझौतावादी समाधान की रणनीति बहुत धीमी और अप्रभावी थी। उन्होंने पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की वकालत की, जिसे बल सहित किसी भी आवश्यक साधनों से हासिल किया जाना था। इसने उन्हें गांधी के विपरीत खड़ा कर दिया, जो अहिंसा और रचनात्मक कार्य में विश्वास रखते थे।
इस आंतरिक संघर्ष का चरमोत्कर्ष 1938 में आया जब बोस को अपने हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने तीव्र औद्योगीकरण और अंग्रेजों के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख के कार्यक्रम की वकालत की, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए समाजवाद और फासीवादी अनुशासन के मेल की कल्पना की। 1939 में, उन्होंने गांधी की इच्छाओं को चुनौती देते हुए फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिन्होंने पट्टाभि सीतारमैया का समर्थन किया था। बोस ने दूसरा कार्यकाल जीता, एक नाटकीय घटना जिसने गांधी के अधिकार को एक मजबूत चुनौती का संकेत दिया।
हालाँकि, जीत अल्पकालिक थी। गांधी के मजबूत विरोध और पूरी कार्यसमिति के इस्तीफे के सामने, बोस खुद को अलग-थलग पाया। बिना किसी समर्थन के, उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे कांग्रेस के पुराने गार्ड के साथ एक अंतिम और अपरिवर्तनीय विभाजन हो गया।
महान पलायन और आज़ाद हिंद फौज का गठन
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ, बोस ने एक अद्वितीय अवसर देखा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, “ब्रिटेन की कठिनाई भारत का अवसर है।” उनका मानना था कि ब्रिटेन की धुरी राष्ट्रों की हार भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जुलाई 1940 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में सख्त नजरबंदी में रखे जाने के बाद, उन्होंने एक साहसिक पलायन की सावधानीपूर्वक योजना बनाई।
19 जनवरी, 1941 को, एक पठान बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में भेष बदलकर, वह अपने सतर्क पहरेदारों से दूर निकल गए। उनकी यात्रा महाकाव्य से कम नहीं थी। वह कार, ट्रेन और पैदल चलकर पेशावर गए, फिर अफगानिस्तान में, और अंततः सोवियत संघ पहुंचे। मास्को से, वह एक राजनयिक इतालवी पासपोर्ट के माध्यम से अप्रैल 1941 में बर्लिन, जर्मनी पहुंचे।
नाजी जर्मनी में, बोस ने एडोल्फ हिटलर का समर्थन मांगा। जबकि नाजी शुरू में अनिश्चित थे, उन्होंने अंततः अपने स्वयं के रणनीतिक कारणों से उनके उद्देश्य का समर्थन करने को सहमति दे दी। बर्लिन में, उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और रोमेल के अफ्रीका कोर द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से भारतीय सेना (इंडियन लीजन) को खड़ा किया। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रचार भाषणों का प्रसारण भी शुरू किया, जिससे उनके शक्तिशाली भाषणों ने भारत में वापस भारतीयों को प्रेरित किया। हालाँकि, वे नाजियों की भारतीय स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की कमी और उनकी नस्लीय विचारधाराओं से निराश हो गए, जो उनके अपने दृष्टिकोण से टकराती थीं।
जब जर्मनी के खिलाफ युद्ध का रुख बदल गया, और दक्षिणपूर्व एशिया में जापानी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बोस ने एक नया रास्ता देखा। फरवरी 1943 में, उन्होंने एक जोखिम भरी तीन-माह की पनडुब्बी यात्रा शुरू की, मेडागास्कर के तट पर एक जर्मन पनडुब्बी से एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित हुए। वह मई 1943 में टोक्यो पहुंचे, जहां उन्हें जापानी नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधान मंत्री हिदेकी तोजो से अधिक उत्साहपूर्ण प्रतिबद्धता मिली।
उनका भाग्योदय का क्षण दक्षिणपूर्व एशिया में आया। सिंगापुर और मलाया के पतन के दौरान जापानियों ने हजारों भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया था। बोस ने उनमें एक मुक्ति सेना की नींव देखी। 4 जुलाई, 1943 को, उन्होंने सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभाली। अगले दिन, उन्हें पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में घोषित किया गया।
21 अक्टूबर, 1943 को उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई, जब उन्होंने आज़ाद हिंद (स्वतंत्र भारत) की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। INA में भारतीय युद्ध बंदियों और दक्षिणपूर्व एशिया में भारतीय प्रवासी समुदायों के नागरिक स्वयंसेवक शामिल थे। बोस इसके सर्वोच्च कमांडर बने।
आईएनए अभियान और इसकी विरासत
बोस के नेतृत्व ने आईएनए में बिजली भर दी। उन्होंने सेना को अपना प्रसिद्ध युद्ध घोष दिया “जय हिंद” (भारत की जीत) और “दिल्ली चलो” (आगे दिल्ली की ओर)। उनकी अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और धुरी राष्ट्रों और उनके सहयोगियों द्वारा मान्यता प्राप्त की।
एक प्रतीकात्मक कदम में, बोस की सरकार ने अपनी मुद्रा, डाक टिकट जारी किए, और झांसी की रानी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट की स्थापना की, जो दुनिया की पहली पूर्णतः महिला पैदल सेना लड़ाकू इकाई थी।
1944 की शुरुआत में, आईएनए ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने के लिए जापानी बलों के साथ मिलकर अपना सैन्य अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य बर्मा से मणिपुर और इंफाल में सीमा पार करना, जनता का विद्रोह भड़काना और ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना था। आईएनए के सैनिकों ने, हालांकि खराब सुसज्जित और अपर्याप्त आपूर्ति में, अत्यधिक साहस के साथ लड़ाई लड़ी। हालाँकि, इंफाल और कोहिमा अभियान की विफलता, मानसून, बीमारी और मित्र देशों की वायु श्रेष्ठता से बढ़कर, एक विनाशकारी हार में हुई। आईएनए को एक क्रूर पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा।
सैन्य विफलता के बावजूद, आईएनए का राजनीतिक प्रभाव गहरा और far-reaching था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने 1945 में दिल्ली के लाल किले पर देशद्रोह के आरोप में पकड़े गए आईएनए सैनिकों पर मुकदमा चलाया। प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाह नवाज खान के मुकदमों ने पूरे भारत में जबरदस्त सार्वजनिक आक्रोश और सहानुभूति पैदा कर दी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें नेहरू और भूलाभाई देसाई शामिल थे, ने प्रसिद्ध रूप से सैनिकों का बचाव किया। व्यापक विरोध और इस बोध ने कि ब्रिटिश भारतीय सेना की निष्ठा को अब स्वीकार नहीं लिया जा सकता, अंग्रेजों को विश्वास दिला दिया कि भारत में उनके दिन गिने-चुने हैं। बोस द्वारा रचित आईएनए गाथा ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर एक घातक प्रहार किया था।
रहस्यमय मृत्यु और स्थायी विरासत
नेताजी के जीवन का अंत रहस्य और विवाद में लिपटा हुआ है। आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया है कि 18 अगस्त, 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद, बोस सोवियत संघ में भागने का प्रयास कर रहे थे। ताइहोकू (ताइपे) में फॉर्मोसा (अब ताइवान) से उड़ान भरने के तुरंत बाद उनका अधिभारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें गंभीर तीसरी डिग्री की जलन हुई और कुछ घंटों बाद एक स्थानीय अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और राख को टोक्यो ले जाया गया और रेन्कोजी मंदिर में रखा गया।
हालाँकि, निर्णायक भौतिक सबूतों की अनुपस्थिति और ब्रिटिश सरकार की उनसे संबंधित फाइलों के आसपास की गोपनीयता ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया कि वह दुर्घटना में नहीं मरे थे। षड्यंत्र के सिद्धांत फैल गए: कि वह सोवियत गुलाग में एक कैदी थे; कि वह “गुमनामी बाबा” नाम के एक संत के रूप में भारत लौट आए या कि वह गोपनीयता में रहते थे।
भारत में कई आधिकारिक समितियों ने उनके गायब होने की जांच की है, लेकिन किसी ने भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया है जो सभी को संतुष्ट कर सके। शाहनवाज समिति (1956) और खोसला आयोग (1970) ने विमान दुर्घटना की कहानी को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (2005) ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि बोस की दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी। भारत सरकार ने तब से सैकड़ों फाइलों को डीक्लासिफाई किया है, लेकिन रहस्य बना हुआ है, जो आदमी की शक्तिशाली और रहस्यमय उपस्थिति का एक प्रमाण है।
सुभाष चंद्र बोस की विरासत जटिल और बहुआयामी है।
- देशभक्त और प्रतीक: उन्हें सर्वोच्च स्तर के राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ, अपना जीवन तक, स्वतंत्रता के कारण के लिए बलिदान कर दिया। उनका जन्मदिन भारत में “पराक्रम दिवस” के रूप में मनाया जाता है।
- सैन्य रणनीतिकार: हालाँकि उनका सैन्य अभियान विफल रहा, आईएनए का अस्तित्व और बाद के लाल किले के मुकदमों ने भारत को पकड़ने के ब्रिटिश संकल्प को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।
- दूरदर्शी नेता: जाति और धार्मिक विभाजनों से मुक्त, एक मजबूत, केंद्रीकृत और समाजवादी भारत पर उनके विचार लगातार प्रेरित करते हैं। उनका नारा “जय हिंद” भारत के राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में अपनाया गया था, और आईएनए का आदर्श वाक्य इत्तेहाद (एकता), इत्माद (विश्वास), कुरबानी (बलिदान) शक्तिशाली बना हुआ है।
- विवादास्पद व्यक्ति: नाजी जर्मनी और साम्राज्यवादी जापान के साथ उनके गठजोड़, फासीवादी शासन जो जबरदस्त अत्याचारों के लिए जिम्मेदार हैं, गहन ऐतिहासिक बहस का विषय बने हुए हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह व्यावहारिक लेकिन नैतिक रूप से संदेहास्पद समझौता था। समर्थकों का तर्क है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ जीवन-मरण के संघर्ष में, मुक्ति के लिए कोई भी उपाय उचित था।
अंत में, सुभाष चंद्र बोस प्रकृति की एक शक्ति थे अत्यधिक जुनून, बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति के एक नेता। उन्होंने अपने समकालीनों से बिल्कुल अलग रास्ता चुना, यह मानते हुए कि उनके दुश्मन का दुश्मन उनका दोस्त हो सकता है। हालाँकि उनके तरीकों पर बहस हुई, लेकिन उनकी देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।
उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षितिज का विस्तार किया, एक सैन्य आयाम पेश किया जिसने ब्रिटिश राज के अंत को तेज कर दिया। नेताजी का जीवन और रहस्यमय गायब होना उनकी जगह केवल इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की स्थायी और शक्तिशाली कल्पना में सुरक्षित कर दिया है जिसे वे मुक्त करना चाहते थे। वे उस आग्नेय, अदम्य देशभक्त बने हुए हैं जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा और इसे हासिल करने के लिए अंतिम कीमत चुकाने को तैयार थे।
अगर आपको हमारी कहानी से जुड़ा कोई सवाल है, तो कृपया लेख के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हम आपको सभी सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य कहानियाँ पढ़ने के लिए द बायो से जुड़े रहें।